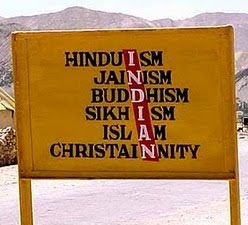विमर्श : नए शब्द
विमर्श : नए शब्द
*
रखने अथवा नामकरण तथा जन प्रचलित शब्द के स्थान पर नया शब्द ‘बनाने´ अथवा ‘गढ़ने´ में अन्तर है। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा शब्द निर्माण पर मेरा टिप्पण था- “उन्होंने जन-प्रचलित शब्दों को अपनाने के स्थान पर संस्कृत का सहारा लेकर शब्द गढ़े। शब्द बनाए नहीं जाते। गढ़े नहीं जाते। लोक के प्रचलन एवं व्यवहार से विकसित होते हैं।” इस पर एक विद्वान ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वह नीचे उद्धृत है- “प्रो. जैन जो कहते हैं, उसे दो अंशों में बाँट कर सोचते हैं। क और ख।
(क) “उन्होंने जन प्रचलित शब्दों को अपनाने के स्थान पर संस्कृत का सहारा लेकर शब्द गढ़े।
(ख) शब्द बनाए नहीं जाते। गढ़े नहीं जाते। लोक के प्रचलन एवं व्यवहार से विकसित होते हैं।”
(क) “जन प्रचलित” - यह जन कोई एक व्यक्ति नहीं है। और अनेक व्यक्ति यदि प्रचलित करते हैं, तो, क्या वे एक ही शब्द जो सर्वमान्य हो, ऐसा शब्द प्रचलित कर सकते हैं?
(क१) और प्रचलित कैसे करेंगे? जब प्रत्येक का अलग शब्द होगा, तो, अराजकता नहीं जन्मेगी? और यदि ऐसा होता है, तो वैचारिक संप्रेषण कैसे किया जाए?
(ख) शब्द बनाए नहीं जाते। गढे नहीं जाते?”।
मैंने विद्वान महोदय की उपर्युक्त आपत्तियों का जो उत्तर दिया वह निम्न है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का ‘नाम रखने´ अथवा ´नामकरण करने’ तथा जन प्रचलित शब्द के स्थान पर नया शब्द ‘बनाने´ अथवा ‘गढ़ने´ में अन्तर है। ये भिन्न ´विचारों’ के वाचक हैं; भिन्न ‘संकल्पनाओं´ के बोधक हैं। आप सम्भवतः भाषाविज्ञान के विशेषज्ञ नहीं हैं, इस कारण आपकी सुविधा के लिए मैं दोनों के
अन्तर एवं भेद को उदाहरणों से स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। “नामकरण” करना तथा जन प्रचलित शब्द के स्थान पर नया शब्द ‘गढ़ना'-
(अ) नामकरण करना अथवा नाम रखना -
(क) व्यक्ति का नामकरण - घर में जब किसी शिशु का जन्म होता है, वह भगवान के घर से कोई नाम लेकर पैदा नहीं होता। उसका ´नामकरण’ होता है। उसका हम नाम रखते हैं। उसके लिए नाम बनाते नहीं हैं। उसके लिए नाम गढ़ते नहीं हैं। जो नाम रखते हैं, वह समाज में उस शिशु के लिए प्रचलित हो जाता है। लोक उसे उसके रखे नाम से पहचानता है। नाम व्यक्तित्व का अंग हो जाता है। नाम व्यक्ति से जुड़ जाता है।
(ख) नई व्यवस्था, नई वस्तु, नए आविष्कार के लिए नामकरण - भारत ने गुलामी की जंजीरों को काटकर स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वाधीन होने के पहले से ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए ‘संविधान सभा´ का गठन कर दिया था। हमारे देश की संविधान सभा ने राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र को ध्यान में रखकर संविधान बनाया। राजतंत्र में सर्वोच्च पद राजा का होता है। लोकतंत्र के लिए उन्होंने ´राष्ट्रपति’ का पद बनाया। राष्ट्रपति शब्द इस कारण प्रचलित हो गया। उसके लिए कोई दूसरा शब्द जनता में प्रचलित नहीं था। पद ही नहीं था तो उसका वाचक कैसे होता। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में इसी कारण बहुत से नए शब्दों का नामकरण किया। उनके लिए लोक में कोई अन्य नाम प्रचलित नहीं थे। आपने अपने टिप्पण में जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनमें से अधिकतर इसी कोटि के अन्तर्गत आते हैं।
कुछ अन्य उदाहरण देखें- (1) भारत की सरकार ने जब पद्म पुरस्कारों की नई योजना बनाई तो पुरस्कारों की तीन श्रेणियाँ बनाई तथा उनके नाम रखे - (अ) पद्म विभूषण (आ) पद्म भूषण (इ) पद्म श्री। इसके लिए कोई अन्य नाम प्रचलित नहीं थे। प्रचलित नहीं थे, क्योंकि ये पुरस्कार ही नहीं थे। इस कारण रखे गए नाम चले। इनका प्रचलन हो गया। (2) भारत की सरकार ने जब पूर्वोत्तर भारत में नए राज्यों का गठन किया तो उनके लिए नाम रखे। (अ) अरुणाचल प्रदेश (आ) मणिपुर (इ) मेघालय (ई) मिज़ोरम (उ) नगालैण्ड आदि। इन नए गठित राज्यों के लिए पहले से कोई शब्द नहीं थे। शब्द इस कारण नहीं थे क्योंकि राज्य ही नहीं थे। इन नए राज्यों का नामकरण किया गया। इन राज्यों को सब इनके नाम से पुकारते हैं। (3) अभी हाल में ‘आन्ध्र प्रदेश´ को दो भागों में बाँटा गया है। एक राज्य का नामकरण किया गया- तेलंगाना । दूसरे राज्य का नामकरण किया गया - सीमान्ध्र। ये नाम चलेंगे। लोक प्रचलित हो जाएँगे। (4) भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चन्द्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष प्रेक्षण उपग्रह का नाम ‘चन्द्रयान´ तथा मंगल पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष प्रेक्षण उपग्रह का नाम ‘मंगलयान´ रखा। इनका नामकरण ´चन्द्रयान’ एवं ‘मंगलयान’ किया। ये नाम चल रहे हैं। संसार की किसी भी देश का वैज्ञानिक जब किसी भी भाषा में इनका उल्लेख करेगा तो उसे ‘चन्द्रयान´ एवं ‘मंगलयान´ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा।
(आ) शब्द बनाना अथवा शब्द गढ़ना- अब मैं शब्द बनाने अथवा शब्द गढ़ने को एक उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। अंग्रेजों ने भारत में ‘रेलवे नेटवर्क´ शुरु किया। रेल की पटरियों का जाल बिछाने का काम किया। रेल से जुड़े अंग्रेजी के सैकड़ों शब्द जन प्रचलित हो गए। उदाहरण देखें- (1) इंजन (2) रेलवे (3) एक्सप्रेस (4) केबिन (5) गॉर्ड (6) स्टेशन (7) जंक्शन (8) टाइम टेबिल (9) टिकट (10) टिकट कलेक्टर (11) डीजल इंजन (12) प्लेटफॉर्म (13) बोगी (14) बुकिंग (15) सिग्नल (16) स्टेशन (17) स्टेशन मास्टर।
इन जैसे जन प्रचलित शब्दों के स्थान पर इनके लिए नए शब्द बनाने अथवा गढ़ने वालों से मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। भारतीय भाषाविज्ञान की महान परम्परा के अध्ययन के बाद मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। आचार्य रघुवीर जी ने जो कार्य किया है वह स्तुत्य है मगर उन्होंने भी अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों को गढ़ा है उनसे सहमत नहीं हूँ। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी के स्थान पर उन्होंने संस्कृत की धातुओं एवं परसर्गों एवं विभक्तियों की सहायता से शब्द बनाया जो उपहास का कारक बना। ऐसे ही उदाहरणों के कारण ´रघुवीरी हिन्दी’ हास्यास्पद हो गई। लोक में रेल ही चलता है और चलेगा। गढ़ा शब्द नहीं चलेगा। इसी संदर्भ में, मेरा मत है कि जो शब्द जन-प्रचलित हैं उनके स्थान पर शब्द गढ़े नहीं। इस विषय पर इलाहाबाद में लेखक के रज्जू भैया से बहुत लम्बे संवाद हुए हैं।
लेखक सन् 1958 से लेकर सन् 1962 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार उसके पिताजी के मित्र श्री केएल गोविल थे। उनके घर पर लेखक की ´संघ के रज्जू भैया’ से अनेक बार मुलाकात हुईं। उनकी सोच यह थी कि हमारे राष्ट्र की मूल धारा एक है और वह धारा अविरल एवं शुद्ध रूप में प्रवाहित है। जो धाराएँ हमारे देश में आक्रांताओं के द्वारा लाई गयीं हैं उन्होंने हमारी राष्ट्र रूपी गंगा को गंदा कर दिया है। हमें उसे निर्मल बनाना है। मेरे दिमाग में उस समय से लेकर अब तक दिनकर की पंक्तियाँ गूँजती रही हैं कि भारतीय संस्कृति समुद्र की तरह है जिसमें अनेक धाराएँ आकर विलीन होती रही हैं। एक दिन हमने रज्जू भैया से निवेदन किया कि आप जिन आगत धाराओं को गंदे नालों के रूप में देखते हैं, हम उनको इस रूप में नहीं देखते। उन समस्त धाराओं को जिन्हें आप गंदे नालों एवं ´मल’ के रूप में देखते हैं उनको हम ‘ऐसे मल´ की श्रेणी में नहीं रख सकते जो हमारी भाषा, धर्म, एवं संस्कृति रूपी गंगा को ´गंदा नाला’ बनाते हैं। आगत धाराएँ हमारी गंगा की मूल स्रोत भागीरथी में आकर मिलने वाली अलकनंदा,धौली गंगा,अलकन्दा, पिंडर और मंदाकिनी धाराओं की श्रेणी में आती हैं। हिन्दी भाषा की प्रकृति और स्वरूप के बारे में भी हमारी सोच यही है। आप नया आविष्कार करें और उसका नामकरण करें, यह ठीक है। जो शब्द जन-प्रचलित हो गए हैं उनके स्थान पर नए शब्द बनाना अथवा गढ़ना श्रम का अपव्यय है। हमें किसी विचार शाखा से अपने को जकड़ना नहीं चाहिए। भाषा की प्रवाहशील प्रकृति को आत्मसात करना चाहिए।
Read More
*
रखने अथवा नामकरण तथा जन प्रचलित शब्द के स्थान पर नया शब्द ‘बनाने´ अथवा ‘गढ़ने´ में अन्तर है। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा शब्द निर्माण पर मेरा टिप्पण था- “उन्होंने जन-प्रचलित शब्दों को अपनाने के स्थान पर संस्कृत का सहारा लेकर शब्द गढ़े। शब्द बनाए नहीं जाते। गढ़े नहीं जाते। लोक के प्रचलन एवं व्यवहार से विकसित होते हैं।” इस पर एक विद्वान ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वह नीचे उद्धृत है- “प्रो. जैन जो कहते हैं, उसे दो अंशों में बाँट कर सोचते हैं। क और ख।
(क) “उन्होंने जन प्रचलित शब्दों को अपनाने के स्थान पर संस्कृत का सहारा लेकर शब्द गढ़े।
(ख) शब्द बनाए नहीं जाते। गढ़े नहीं जाते। लोक के प्रचलन एवं व्यवहार से विकसित होते हैं।”
(क) “जन प्रचलित” - यह जन कोई एक व्यक्ति नहीं है। और अनेक व्यक्ति यदि प्रचलित करते हैं, तो, क्या वे एक ही शब्द जो सर्वमान्य हो, ऐसा शब्द प्रचलित कर सकते हैं?
(क१) और प्रचलित कैसे करेंगे? जब प्रत्येक का अलग शब्द होगा, तो, अराजकता नहीं जन्मेगी? और यदि ऐसा होता है, तो वैचारिक संप्रेषण कैसे किया जाए?
(ख) शब्द बनाए नहीं जाते। गढे नहीं जाते?”।
मैंने विद्वान महोदय की उपर्युक्त आपत्तियों का जो उत्तर दिया वह निम्न है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का ‘नाम रखने´ अथवा ´नामकरण करने’ तथा जन प्रचलित शब्द के स्थान पर नया शब्द ‘बनाने´ अथवा ‘गढ़ने´ में अन्तर है। ये भिन्न ´विचारों’ के वाचक हैं; भिन्न ‘संकल्पनाओं´ के बोधक हैं। आप सम्भवतः भाषाविज्ञान के विशेषज्ञ नहीं हैं, इस कारण आपकी सुविधा के लिए मैं दोनों के
अन्तर एवं भेद को उदाहरणों से स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। “नामकरण” करना तथा जन प्रचलित शब्द के स्थान पर नया शब्द ‘गढ़ना'-
(अ) नामकरण करना अथवा नाम रखना -
(क) व्यक्ति का नामकरण - घर में जब किसी शिशु का जन्म होता है, वह भगवान के घर से कोई नाम लेकर पैदा नहीं होता। उसका ´नामकरण’ होता है। उसका हम नाम रखते हैं। उसके लिए नाम बनाते नहीं हैं। उसके लिए नाम गढ़ते नहीं हैं। जो नाम रखते हैं, वह समाज में उस शिशु के लिए प्रचलित हो जाता है। लोक उसे उसके रखे नाम से पहचानता है। नाम व्यक्तित्व का अंग हो जाता है। नाम व्यक्ति से जुड़ जाता है।
(ख) नई व्यवस्था, नई वस्तु, नए आविष्कार के लिए नामकरण - भारत ने गुलामी की जंजीरों को काटकर स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वाधीन होने के पहले से ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए ‘संविधान सभा´ का गठन कर दिया था। हमारे देश की संविधान सभा ने राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र को ध्यान में रखकर संविधान बनाया। राजतंत्र में सर्वोच्च पद राजा का होता है। लोकतंत्र के लिए उन्होंने ´राष्ट्रपति’ का पद बनाया। राष्ट्रपति शब्द इस कारण प्रचलित हो गया। उसके लिए कोई दूसरा शब्द जनता में प्रचलित नहीं था। पद ही नहीं था तो उसका वाचक कैसे होता। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में इसी कारण बहुत से नए शब्दों का नामकरण किया। उनके लिए लोक में कोई अन्य नाम प्रचलित नहीं थे। आपने अपने टिप्पण में जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनमें से अधिकतर इसी कोटि के अन्तर्गत आते हैं।
कुछ अन्य उदाहरण देखें- (1) भारत की सरकार ने जब पद्म पुरस्कारों की नई योजना बनाई तो पुरस्कारों की तीन श्रेणियाँ बनाई तथा उनके नाम रखे - (अ) पद्म विभूषण (आ) पद्म भूषण (इ) पद्म श्री। इसके लिए कोई अन्य नाम प्रचलित नहीं थे। प्रचलित नहीं थे, क्योंकि ये पुरस्कार ही नहीं थे। इस कारण रखे गए नाम चले। इनका प्रचलन हो गया। (2) भारत की सरकार ने जब पूर्वोत्तर भारत में नए राज्यों का गठन किया तो उनके लिए नाम रखे। (अ) अरुणाचल प्रदेश (आ) मणिपुर (इ) मेघालय (ई) मिज़ोरम (उ) नगालैण्ड आदि। इन नए गठित राज्यों के लिए पहले से कोई शब्द नहीं थे। शब्द इस कारण नहीं थे क्योंकि राज्य ही नहीं थे। इन नए राज्यों का नामकरण किया गया। इन राज्यों को सब इनके नाम से पुकारते हैं। (3) अभी हाल में ‘आन्ध्र प्रदेश´ को दो भागों में बाँटा गया है। एक राज्य का नामकरण किया गया- तेलंगाना । दूसरे राज्य का नामकरण किया गया - सीमान्ध्र। ये नाम चलेंगे। लोक प्रचलित हो जाएँगे। (4) भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चन्द्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष प्रेक्षण उपग्रह का नाम ‘चन्द्रयान´ तथा मंगल पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष प्रेक्षण उपग्रह का नाम ‘मंगलयान´ रखा। इनका नामकरण ´चन्द्रयान’ एवं ‘मंगलयान’ किया। ये नाम चल रहे हैं। संसार की किसी भी देश का वैज्ञानिक जब किसी भी भाषा में इनका उल्लेख करेगा तो उसे ‘चन्द्रयान´ एवं ‘मंगलयान´ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा।
(आ) शब्द बनाना अथवा शब्द गढ़ना- अब मैं शब्द बनाने अथवा शब्द गढ़ने को एक उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। अंग्रेजों ने भारत में ‘रेलवे नेटवर्क´ शुरु किया। रेल की पटरियों का जाल बिछाने का काम किया। रेल से जुड़े अंग्रेजी के सैकड़ों शब्द जन प्रचलित हो गए। उदाहरण देखें- (1) इंजन (2) रेलवे (3) एक्सप्रेस (4) केबिन (5) गॉर्ड (6) स्टेशन (7) जंक्शन (8) टाइम टेबिल (9) टिकट (10) टिकट कलेक्टर (11) डीजल इंजन (12) प्लेटफॉर्म (13) बोगी (14) बुकिंग (15) सिग्नल (16) स्टेशन (17) स्टेशन मास्टर।
इन जैसे जन प्रचलित शब्दों के स्थान पर इनके लिए नए शब्द बनाने अथवा गढ़ने वालों से मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। भारतीय भाषाविज्ञान की महान परम्परा के अध्ययन के बाद मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। आचार्य रघुवीर जी ने जो कार्य किया है वह स्तुत्य है मगर उन्होंने भी अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों को गढ़ा है उनसे सहमत नहीं हूँ। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी के स्थान पर उन्होंने संस्कृत की धातुओं एवं परसर्गों एवं विभक्तियों की सहायता से शब्द बनाया जो उपहास का कारक बना। ऐसे ही उदाहरणों के कारण ´रघुवीरी हिन्दी’ हास्यास्पद हो गई। लोक में रेल ही चलता है और चलेगा। गढ़ा शब्द नहीं चलेगा। इसी संदर्भ में, मेरा मत है कि जो शब्द जन-प्रचलित हैं उनके स्थान पर शब्द गढ़े नहीं। इस विषय पर इलाहाबाद में लेखक के रज्जू भैया से बहुत लम्बे संवाद हुए हैं।
लेखक सन् 1958 से लेकर सन् 1962 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार उसके पिताजी के मित्र श्री केएल गोविल थे। उनके घर पर लेखक की ´संघ के रज्जू भैया’ से अनेक बार मुलाकात हुईं। उनकी सोच यह थी कि हमारे राष्ट्र की मूल धारा एक है और वह धारा अविरल एवं शुद्ध रूप में प्रवाहित है। जो धाराएँ हमारे देश में आक्रांताओं के द्वारा लाई गयीं हैं उन्होंने हमारी राष्ट्र रूपी गंगा को गंदा कर दिया है। हमें उसे निर्मल बनाना है। मेरे दिमाग में उस समय से लेकर अब तक दिनकर की पंक्तियाँ गूँजती रही हैं कि भारतीय संस्कृति समुद्र की तरह है जिसमें अनेक धाराएँ आकर विलीन होती रही हैं। एक दिन हमने रज्जू भैया से निवेदन किया कि आप जिन आगत धाराओं को गंदे नालों के रूप में देखते हैं, हम उनको इस रूप में नहीं देखते। उन समस्त धाराओं को जिन्हें आप गंदे नालों एवं ´मल’ के रूप में देखते हैं उनको हम ‘ऐसे मल´ की श्रेणी में नहीं रख सकते जो हमारी भाषा, धर्म, एवं संस्कृति रूपी गंगा को ´गंदा नाला’ बनाते हैं। आगत धाराएँ हमारी गंगा की मूल स्रोत भागीरथी में आकर मिलने वाली अलकनंदा,धौली गंगा,अलकन्दा, पिंडर और मंदाकिनी धाराओं की श्रेणी में आती हैं। हिन्दी भाषा की प्रकृति और स्वरूप के बारे में भी हमारी सोच यही है। आप नया आविष्कार करें और उसका नामकरण करें, यह ठीक है। जो शब्द जन-प्रचलित हो गए हैं उनके स्थान पर नए शब्द बनाना अथवा गढ़ना श्रम का अपव्यय है। हमें किसी विचार शाखा से अपने को जकड़ना नहीं चाहिए। भाषा की प्रवाहशील प्रकृति को आत्मसात करना चाहिए।

.png) Hire Us
Hire Us