लेख :
श्रीकृष्ण के जीवन में मानव मूल्य
आचार्य संजीव वर्मा 'सलिल'
*
श्रीकृष्ण का उद्भव जिस काल में हुआ था वह नैतिकता के संक्रमण और पराभव का काल था। भारत की प्रचलित-पुरातन गणतंत्रात्मक शासन पद्धति संकट में थी। राजे-महाराजे अपने राजधर्म, प्रजा के प्रति कर्तव्य तथा स्वजनों के प्रति दायित्व का पालन नहीं कर रहे थे। शासकों के मनमाने आचरण से पीड़ित प्रजा त्राहि-त्राहि कर रही थी। विद्वद्वर्ग शासकों से आर्थिक सहायता के बदले उनके क्रीत दास की तरह आचरण कर रहा था। आश्रम और गुरुकुल लोकाश्रित रहने के स्थान पर राज्याश्रित होते जा रहे थे। समाज पारस्परिक द्वेष और फूट का शिकार था। सत्ता से असहमत रहनेवालों की खैर नहीं थी। अधिकांश राजा अपने अहंकार की बलिवेदी पर जन-हित की बलि दे रहे थे। युवा राजकुमार सम्राटों की उपेक्षा कर मनमानी कर रहे थे। जनमत की उपेक्षा, राजमद, भोग-विलास, स्वार्थपरता, संकीर्ण परिवार हित को देश-समाज पर वरीयता, राष्ट्रीय भावना का अभाव, जन सामान्य की असुरक्षा व शोषण की प्रवृत्तियों के कारण समूचा परिदृश्य लोक हितैषी ऋषि-मुनियों और समाज सुधारकों लिए चिंता का कारण था। शोषित जनगण त्रस्त था। सात्विक प्रवृत्ति के सज्जन परमात्मा को यादकर उद्धार करने की प्रार्थना कर रहे थे।
कृष्ण जन्म के पूर्व सामाजिक स्थिति
कृष्ण जन्म के पूर्व हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन रहे राजा शांतनु ने गंगा से विवाह अमानवीय शर्त को स्वीकार कर किया था। जिसका प्रतिफल उनके पुत्रों को गंगा नदी में बहाये जाने से हुआ। अंतिम पुत्र देवव्रत का जीवन बचाने का मूल्य उन्हें अपनी पत्नी को गँवाकर चुकाना पड़ा। वृद्धावस्था में भी उनकी वासना शांत नहीं हो सकी थी। वे अपनी पुत्री से भी कम उम्र की सुन्दरी सत्यवती पर मुग्ध हो गए। उन्हें संतुष्ट करने के लिए देवव्रत को सत्यवती के पालक कैवर्त की अनुचित शर्तों के आगे आत्मसमर्पण कर आजीवन अविवाहित रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। सत्यवती कौमार्यावस्था में ऋषि पाराशर के साथ दैहिक संबंध बना चुकी थी जिससे उत्पन्न पुत्र वेद व्यास थे। शांतनु से उत्पन्न सत्यवती का प्रथम पुत्र चित्रांगद गंधर्व द्वारा मारा गया, शारीरिक रूप से दुर्बल दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह हेतु भीष्म (देवव्रत) ने काशिराज की ३ कन्याओं का बलात् अपहरण कर लिया जिसे किसी भी आधार पर उचित नहीं कहा जा सकता। अनैतिक आचरण यही नहीं रुका। विचित्रवीर्य की २ विधवाओं को उनके पिता की उम्र के महर्षि वेद व्यास से पुत्र उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया गया। फलत:, एक पुत्र नेत्रहीन और दूसरा पाण्डु रोगग्रस्त हुआ। ऋषि तथा विवाहित होते हुए भी व्यास ने अपने सौतेले भाई की विधवाओं से संतति उत्पत्ति करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यही नहीं व्यास ने दासी से भी बिना दैहिक संबंध बनाया जिससे उत्पन्न पुत्र विदुर थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ विवाह के लिए भीष्म ने पुनः शक्ति के बल पर गांधार राजकुमारी को बाध्य किया। पाण्डु की पत्नी बनी पृथा (कुंती) भी कौमार्यावस्था में पुत्र (कर्ण) को जन्म देकर, उसे त्याग चुकी थीं। इन अनैतिक आचरणों का दुष्परिणाम अंतत: भयानक युद्ध और विनाश के रूप में हुआ।
कृष्ण जन्म के पूर्व पांचाल नरेश द्रुपद और उनके गुरुभाई द्रोण के बीच वैमनस्य हो चुका था जिसका कारण द्रुपद द्वारा वचनभंग तथा द्रोण द्वारा सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा थी। शक्तिशाली जरासंध, कालयवन तथा अन्य नरेश नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों के विपरीत आचरण और भोग-विलास कर रहे थे जिसके कारण सामान्य जन संत्रस्त थे।
श्रीकृष्ण के जन्म के पूर्व मथुरा के शासक कंस ने अपने वृद्ध अग्रसेन पिता से सिंहासन छीन लिया था तथा अपनी चचेरी बहिन देवकी और बहनोई वासुदेव को न केवल कैद कर लिया था अपितु उनकी संतानों का वध कर रहा था क्योंकि उसे यह भय था कि देवकी की आठवाँ पुत्र उसका वध कर देगा। यह भय इसलिए उत्पन्न हुआ कि नारद ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। किसी भविष्यवाणी की सत्यता उसके सत्य होने के पूर्व निश्चित नहीं हो सकती। किसी मतिमान व्यक्ति को भविष्यवाणी सुनकर भावी के प्रति सजग होकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर लेना चाहिए। जन्म लेने के साथ ही जीव की मृत्यु होना भी निश्चित हो जाता है। अत:, भविष्यवाणी किसी को कैद करने या उसकी संतानों का वध करने का उचित कारण नहीं हो सकती। शासक अपनी प्रजा के प्रति विशेष रूप से कर्तव्यबद्ध होता है। बहिन और बहनोई के प्रति भाई और साले का विशेष दयित्व होता है। कंस ने अपने कर्तव्य की पूरी तरह अवहेलना की। एक शासक से अपेक्षित होता है कि वह निडरता और निर्भीकता के साथ अपने पद के साथ न्याय करे। कंस इस निकष पर पूरी तरह असफल रहा। कंस के जीवन के प्रति अंध मोह को स्वाभाविक मानें तो भी पहली सातों संतानों की हत्या को किसी तरह न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता चूँकि उनसे कंस को कोई खतरा नहीं था।
जरासंध चक्रवर्ती बनने की अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने हेतु कंस, शल्य, शाल्व आदि अत्याचारी नृपों के साथ दुरभिसंधि कर जन-गण का शोषण करने-कराने में सहयोग कर रहा था। कालयवन भी अधर्मी शासन पद्धति का अनुगामी था।
बेटियों बहिनों के उनकी मनोकामना के विपरीत तथा राजनैतिक हानि-लाभ को दृष्टि में रखकर किए जा रहे थे। नारी का सौदा करने की यह मनोवृत्ति अंतत: द्वेष और पतन का कारण बनी। स्पष्ट है कि इस काल में कन्याओं की इच्छा का कोई महत्व नहीं था। द्रौपदी जैसी प्रतिभाशाली और मुखरा कन्या को भी अपने पिता राजा द्रुपद की बैर भावना संतुष्ट करने के लिए निमित्त बनना पड़ा। अपनी मनोकामना के विपरीत उसे पाँच पांडवों से विवाह करने के लिए बाध्य पड़ा। जन सामान्य क्रूर तथा निरंकुश राजाओं की मनमानी से त्रस्त हो चुकी थी।
कृष्ण - काल की सामाजिक स्थिति
कृष्ण का काल पुरातन मूल्यों के विघटन तथा नव मूल्यों के सृजन का मध्य काल था। उक्त से स्पष्ट है कि 'राजा करे सो न्याय' का बोलबाला हो रहा था। सामान्य जन शासन-प्रशासन, सबल, समृद्ध और समझदार (प्रबुद्ध, विद्वान्, पंडित) द्वारा 'गरीब की लुगाई, गाँव की भौजाई' की तरह शोषित किया रहा था। इंद्र द्वारा बलात कर संग्रहण, कंस के इंगित पर पूतना, तृणावर्त, कुशावर्त द्वारा बालक कृष्ण की हत्या के प्रयास, कंसवध के पश्चात् जरासंध द्वारा मथुरा और कृष्ण-बलराम को नष्ट करने की कोशिश, कौरवों द्वारा पांडवों के न्यायोचित अधिकार का अपहरण, परशुराम द्वारा कर्ण के साथ तथा द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य के साथ अन्याय आदि प्रांगण से स्पष्ट होता है 'जिसकी लाठी उसकी भैंस', 'समरथ को नहीं दोष गोसाईं ' आदि मुहावरे कृष्ण-कालिक सामाजिक स्थिति को इंगित करते हैं। अशक्त गण प्रणाली और निरंकुश राजतंत्र का प्रतीति कृष्ण को शैशव से होने लगी थी। गोकुल के गो-उत्पादों को राजा कंस को भेजने की विवशता, इंद्र द्वारा गोकुल की समृद्धि का शोषण देखते हुए कृष्ण ने बचपन में प्रवेश किया।
कृष्ण का संघर्ष
जन्म के साथ ही कृष्ण का जीवन संघर्ष आरम्भ हो गया था। मैथिलीशरण गुप्त जी ने पंचवटी में लिखा है-
जितने कष्ट-कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला
गौरव-गंध उन्हें उतना ही यत्र-तत्र सर्वत्र मिला
ये पंक्तियाँ श्री कृष्ण के सन्दर्भ में पूरी तरह सटीक हैं। जन्म के तुरंत पश्चात् शिशु कृष्ण को येन-केन-प्रकारेण कंस के कारागृह से गोकुल ले जाया गया ताकि उनकी प्राण रक्षा की जा सके। कृष्ण ने पय-पान की शैशवावस्था में ही पूतना के चंगुल से न केवल अपने प्राण बचाए अपितु पूतना को देह त्यागने के लिए विवश कर दिया। यमलार्जुन प्रसंग कृष्ण की सजगता और जीवट की साक्षी देता है। कालिय नाग को नाथ कर गोकुल से पलायन हेतु विवश कर कृष्ण ने जन सामान्य को निरापद करने के लिए जान की बाजी लगाने का मनोबल और युक्ति का प्रदर्शन किया। देवराज द्वारा इंद्र पूजा के नाम पर बलात जन-धन अधिग्रहण का विरोध कर कृष्ण ने गोकुल के जनगण में पारंपरिक शोषण का विरोध करने की मानसिकता उत्पन्न कर एक सफल जनान्दोलन का नेतृत्व किया। पारिस्थितिक वैषम्य से जूझते हुए, जनगण ही नहीं, पशुधन की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने प्राकृतिक संसाधनों का सम्यक उपयोग किया और जनसहयोग प्राप्त किया। विश्व में ऐसा दूसरा प्रसंग नहीं है जहाँ किसी जन समस्या के समाधान हेतु हुए जनांदोलन का सफल नेतृत्व किसी बालक ने किया हो और उसके पिता-पितामह आदि ने अनुकरण किया हो।
किशोर कृष्ण को गोकुल छोड़कर मथुरा पहुँचने के पीछे क्रूर मथुरापति कंस की आज्ञा थी। नैतिकता को ताक में रखकर कृष्ण बलराम को समाप्त करने के प्रयास किए जाते रहे। अत्याचारों त्रस्त कृष्ण को कंस का वध करना ही पड़ा किंतु इससे कृष्ण के जीवन की समस्या का अंत नहीं हुआ। कंस का श्वसुर महाबलवान जरासंध उनका कट्टर दुश्मन हो गया। जरासंध के आक्रमणों से बचने के लिए कृष्ण को सभी यादवों को लेकर सुदूर समुद्रतट पर जाना पड़ा जहाँ उन्होंने असाधारण सामर्थ्य का परिचय देते हुए द्वारिका नगरी का निर्माण किया।
कृष्ण के जीवन मूल्य
श्री कृष्ण ने अपने जन्म और समकालिक जीवनमूल्यों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। एक समाज सुधारक श्री कृष्ण का अवदान असाधारण ही नहीं अद्वितीय भी है। बचपन में ही सार्वजनिक स्थल पर निर्वस्त्र स्नान करने की कुप्रथा का शमन कृष्ण ने गोपिकाओं के वस्त्र हरण कर किया। इंद्र द्वारा शोषण का अंत इंद्र-पूजा बंद कराकर क्या गया। इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने प्रकृति पर्यावरण का आश्रय लिया तथा गोवर्धन और गौ के पूजन का श्री गणेश कराया। सामाजिक भेदभाव और ऊँच-नीच मिटाने के लिए कृष्ण ने रास लीला का आयोजन किया जिसमें आयु, जाति, शिक्षा, वर्ण, लिंग आदि का कोई भेदभाव नहीं था। गौ पालन के द्वारा कृष्ण ने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा की। कृषि और गौपालन कर रहे यादव कंस और इंद्र को दोहरा कर चुका रहे थे। कृष्ण ने इस आर्थिक शोषण के विरुद्ध जनमत को तैयार किया और उनका नेतृत्व कर शोषण से मुक्ति दिलाई।
कंस वध के पश्चात् कृष्ण अवसर मिलने पर भी मथुरा नरेश नहीं बने, न अपने पिता या अग्रज बनाया। उन्होंने कंस के पिता वृद्ध उग्रसेन को ही सर्व सम्मति से मथुराधिपति बनाया जिनसे कंस ने सत्ता छीन ली थी। कृष्ण ने राज्यतंत्र को अस्वीकार कर गणतंत्रात्मक पद्धति को पुनः स्थापित किया। द्वारिका में भी कृष्ण ने यही पद्धति अपनाई।
नारियों का सम्मान
कृष्ण ने नारियों को उचित गरिमा देते हुए, उनके निर्णयों का सदा सम्मान किया। यशोदा पहली स्त्री थीं जीवन में आईं। शिशु से किशोर होते कृष्ण मैया को स्नेह-सम्मान दें यह स्वाभाविक है किंतु गोकुल छोड़ने के बाद यह विदित होने पर भी कि यशोदा सगी माँ नहीं हैं, कृष्ण ने सदा उन्हें मैया ही माना। देवकी जन्मदात्री थीं जिन्होंने जन्मते ही कृष्ण को त्याग दिया था तथापि कृष्ण ने उन्हें भी माँ ही माना। राधा कृष्ण के जीवन में थीं या नहीं यह विवादास्पद हैं परंतु उम्र में पर्याप्त बड़ी राधा को अपनी आद्य शक्ति के रूप में स्वीकारा कृष्ण ने। रास जैसे प्रसंग होने के बाद भी कृष्ण ने कभी राधा की पवित्रता व् सम्मान पर आँच न आने दी। यहाँ तक की बृज की बड़ी-छोटी गोपियाँ अपने घरों और स्वजनों की अनुमति के बिना कृष्ण की लीला सहयोगी हुईं, उनकी शुचिता भी कृष्ण ने बनाये रखी।
मथुरा में कुबड़ेपन कारण पति द्वारा उपेक्षित कंस की दासी कुब्जा की व्याधि मिटाकर उसे सम्मान देने के लिए कृष्ण उसके घर भी गए। अपने शत्रु रुक्मी की बहिन रुक्मिणी की मनोकामना पूरी करने के लिए रुक्मी, जरासंध, शिशुपाल आदि के विरोध की परवाह नहीं की और रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया। सूर्यसुता कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करते हुए कृष्ण ने उन्हें अर्धांगिनी बनाया। अवंतिका की राजकुमारी मित्रवृंदा की इच्छापूर्ति हेतु कृष्ण ने स्वयंवर में भाग लेकर उन्हें ग्रहण किया। काशीनरेश नग्नजित तनया सत्या की सम्मान रक्षा के लिए कृष्ण ने सात वृषभों को एक साथ नाथने का असाधारण पराक्रम दिखाया। स्यमन्तक मणि हेतु ऋक्षराज जामवंत से युद्ध होने के बाद भी उनकी पुत्री जामवती का सम्मान करते हुए कृष्ण ने उनसे विवाह किया। गय नरेश ऋतुसुकृत की आत्मजा रोहिणी की मान रक्षा हेतु कृष्ण ने उनका पाणिग्रहण किया। कृष्ण पर उनके विरोधी यादव सामंत सत्राजित ने स्यमन्तक मणि की चोरी का आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को धुल में मिलाने का दुष्प्रयास किया। इसके बाद भी उसकी पुत्री सत्यभाभा के मनोभावों को प्रतिष्ठा देते हुए कृष्ण ने उन्हें धर्मपत्नी स्वीकार किया। लक्ष्मणा तथा शैव्या को भी कृष्ण से प्रेम हुआ और कृष्ण ने उन्हें पत्नी की प्रतिष्ठा दी। यही नहीं नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई १६००० स्त्रिओं को मुक्त करने के बाद शोषण से बचाने और सामाजिक प्रतिष्ठा देने के लिए कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नि स्वीकार किया।
अपनी सखी याज्ञसैनी द्रौपदी के मान-सम्मान व प्रतिष्ठा हेतु कृष्ण ने हर संभव उपाय किए। कौरवों द्वारा चीरहरण का दुष्प्रयास कृष्ण ने ही असफल किया।
अपनी छोटी बहिन सुभद्रा का अर्जुन के प्रति लगाव देखते हुए कृष्ण ने बलराम के विरोध को दरकिनार करते हुए उसे अर्जुन के साथ भागने में सहायता की। पांडवों को वनवास मिलने पर कृष्ण ने सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को द्वारिका में ही रखा तथा श्रेष्ठ प्रशिक्षण की व्यवस्था की।
मित्रता का निर्वहन
श्रीकृष्ण प्रणीत मानव मूल्यों में मित्रता का अमित स्थान है। बाल मित्र सुदामा की दरिद्रता का कृष्ण ने कभी उपहास नहीं किया जबकि द्रुपद ने अपने बाल मित्र द्रोण की उपेक्षा कर अपने विनाश को आमंत्रित किया। कृष्ण ने सुदामा के आने पर उनके पद-प्रक्षालन कर, अपने आसन पर बैठाकर सर्वोच्च सम्मान दिया तथा यथेष्ठ आर्थिक सहायता बिना बताए की। यह आचरण द्रुपद ने द्रोण के साथ किया होता तो इतिहास वह न होता जो हुआ जो हुआ ।
मित्रता का निर्वहन
श्रीकृष्ण प्रणीत मानव मूल्यों में मित्रता का अमित स्थान है। बाल मित्र सुदामा की दरिद्रता का कृष्ण ने कभी उपहास नहीं किया जबकि द्रुपद ने अपने बाल मित्र द्रोण की उपेक्षा कर अपने विनाश को आमंत्रित किया। कृष्ण ने सुदामा के आने पर उनके पद-प्रक्षालन कर, अपने आसन पर बैठाकर सर्वोच्च सम्मान दिया तथा यथेष्ठ आर्थिक सहायता बिना बताए की। यह आचरण द्रुपद ने द्रोण के साथ किया होता तो इतिहास वह न होता जो हुआ। कृष्ण ने राधा, उद्धव, सात्यकि, द्रौपदी, अर्जुन आदि के साथ सखा धर्म का निर्वहन कर उनकी समस्याओं का समाधान खोजा, उन्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का अवसर दिया तथा उनके अनेक संकटों का सामना स्वयं किया।
लोकमत का सम्मान
कृष्ण ने स्थापित बलशाली सम्राटों से जूझते हुए लोकमत को हमेशा मान्यता दी। निरंकुश राजशक्ति द्वारा जान सामान्य का दमन होते देख कृष्ण ने अपने-परायों का भेद किया। वे केवल अपने जनपद के जनगण तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने निकट ही नहीं सुदूर राजाओं में भी राजमद में डूबे सत्तासीनों द्वारा जनहित की उपेक्षा किये जाने पर उन्हें दंडित किया या कराया। निरंकुश शासकों का नाश करते समय कृष्ण ने प्रजा के जान-माल की रक्षा को वरीयता दी। जरासंध और कालयवन जैसे सबल-प्रबल शत्रुओं का नाश उन्होंने इस प्रकार किया कि जनगण को लेशमात्र भी हानि नहीं हुई।
राष्ट्रीय हितों को वरीयता
कृष्ण ने देश में विदेश वणिकों तथा राजाओं द्वारा सत्तासीन होने को देश हित में बाधक मानते हुए उनका विरोध ही नहीं अपितु समूल उन्मूलन किया और उन्हें इस प्रकार खदेड़ा कि कृष्ण युग के पश्चात् भी सदियों तक वे भारत में प्रवेश नहीं कर सके। मथुरा के यादवों को द्वारिका में बसने के पीछे कृष का लक्ष्य विदेशी वणिकों और धनपतियों द्वारा अधिपत्य किये जा चुके क्षेत्र को बचाना भी था। कृष्ण ने देश के सागर तटों को सुरक्षित किया। अनार्य सभ्यताओं को प्रवेश न करने देकर कृष्ण ने वैदिक आर्य जीवन मूल्यों को नवजीवन दिया।
नवमूल्य स्थापना
कृष्ण ने देश-काल-परिस्थितितयों के अनुकूल नव जीवन मूल्यों को स्थापित किया और अपनाया। द्रौपदी स्वयंवर के पश्चात उन्होंने पाँच पांडवों की एक पत्नी को मान्यता दी, उसे धर्मानुकूल भी बताया तथा बहुपतियों के कारण द्रौपदी की अवमानना करने पर दुर्योधन और कर्ण को कभी क्षमा न कर, उनके नाश में सहायक बने। राजनैतिक संबंध स्थापित करने हेतु बिना सहमति राजकन्याओं के विवाह किये जाने को चुनौती देते हुए कृष्ण ने कन्या की मनोकामना को वरीयता दी। परंपरा भंजन करते हुए रुक्मिणी का विवाह पितृगृह में न कर श्वसुरालय द्वारिका में संपन्न कराया।
कृष्ण ने पारिवारिक संबंधियों में उन्हीं को मान्यता दी जो नैतिक आचरण कर रहे थें। धृतराष्ट्र और पाण्डु के पुत्रों के साथ समान संबंध होते हुए भी क्रुद्ध ने अनीति कर रहे कौरवों का विरोध कर पांडवों का समर्थन किया और अपने अग्रज बलराम के मत को भी इन्हीं माना।
परिस्थितियों के चक्रव्यूह में कृष्ण कभी किंकर्तव्यविमूढ़ नहीं हुए। उन्होंने 'लक्ष्य पर दृष्टि रखो, मार्ग पर नहीं' के सिद्धांत को अपनाया। कुरुक्षेत्र में भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि तथा उसके पूर्व जरासंध, कालयवन आदि का विनाश तभी हो सका जब कृष्ण ने बड़ी बुराई के नाश हेतु छोटी बुराई से परहेज नहीं किया। यदि यह नीति सीमान्त प्रदेशों था राजस्थान के नरेश अपना सके होते तो भारत में मुगलों का प्रवेश ही न होता।
इतिहास साक्षी है कि कृष्ण की नीति, आचरण तथा विचार में कोई भेद नहीं था। वे कभी भी स्वहित से संचालित नहीं थे। उनकी वरीयता सर्व हित, सामान्य हित, समाज हित और सर्वोपरि राष्ट्र हित ही था। कृष्ण ने वैश्विकता को भी राष्ट्र से पहले नहीं माना। जब जब देश के हितों पर विदेशियों के कारण आँच आई कृष्ण ने विदेशियों का जड़-मूल से सफाया कर दिया। सारत:, यह स्पष्ट है कि कृष्ण कृष्ण द्वारा अपनाये गए जीवन मूल्य न केवल मानव अपितु राष्ट्र और विश्व के हित में स्थापित की गयी ऐसी विरासत है जो किसी देश-काल में भुलाई न जा सकेगी।
***
संपर्क : विश्ववाणी हिंदी संस्थान, ४०१ विजय अपार्टमेंट, नेपियर टाउन जबलपुर ४८२००१,
चलभाष ९४२५१८३२४४, ईमेल salil.sanjiv@gmail.com

.png) Hire Us
Hire Us


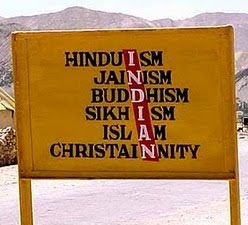
0 पाठकों ने अपनी राय दी है, कृपया आप भी दें!