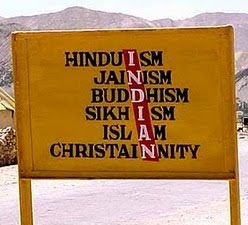जन्नत के बारे में ग़ालिब के ख़याल की हक़ीक़त Standard scale for moral values
ग़ालिब का शेर
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन
दिल के बहलाने को गा़लिब ये ख़याल अच्छा है
 |
| दिल्ली में आपका भाई अनवर जमाल |
 |
| ग़ालिब के बुत के पास आपका भाई अनवर जमाल |
एक आम ग़लती
भाई अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने भी एक बार फिर इस शेर को जब इन्हीं अर्थों में कहा तो मुझे लगा कि कुछ बात ग़ालिब की शायरी और उसके भाव कहना वक्त की ज़रूरत है।
भाई अमरेंद्र जी ! आप आस्ति-नास्तिक, संशयवादी या कुछ और जो भी आप होना चाहें, बेशक हो सकते हैं और अगर आप अपने नज़रिये को अपने शब्दों में कहेंगे तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी केवल आपकी अपनी ही होगी। आप एक साहित्यकार हैं और आप जानते हैं कि किसी भी साहित्यकार के शब्दों से उसी के भाव को ग्रहण करना चाहिए। उसके शब्दों में अपने भाव को अध्यारोपित करना उस साहित्यकार के साथ ज़ुल्म होता है। आपने ऐसा ही कुछ उर्दू शायर ग़ालिब के साथ किया है। आप हिंदी के साहित्यकार हैं। अफ़सोस कि मैं अभी तक आपको पढ़ नहीं पाया हूं लेकिन आपकी पृष्ठभूमि बता रही है, आपके बारे में लोगों की गवाही बता रही है कि आप एक अच्छे साहित्यकार हैं। इसके बावजूद यह भी सच है कि आप उर्दू नहीं जानते। आप यह भी जानते हैं कि किसी साहित्यकार के साहित्य को ठीक से समझने के लिए मात्र भाषा का ज्ञान ही काफ़ी नहीं हुआ करता बल्कि उसके साथ दूसरी कई और भी चीज़ें दरकार होती हैं। जिनमें से एक यह भी है कि साहित्यकार की मनोदशा और उसके व्यक्तित्व को भी जाना समझा जाए, उसके जीवन के पहलुओं को भी सामने रखा जाए।
ग़ालिब की ज़िंदगी के कुछ पहलू
ग़ालिब का पूरा नाम असदुल्लाह था और उनका तख़ल्लुस पहले ‘असद‘ था बाद में ‘ग़ालिब‘ रखा। असदुल्लाह का अर्थ है अल्लाह का शेर और असद का अर्थ होता है शेर। उनका नाम उनके वालिदैन ने रखा था जिससे पता चलता है कि वे ईश्वर के वुजूद पर यक़ीन भी रखते थे और चाहते थे कि उनका बच्चा भी नेकी के रास्ते पर चले। मिर्ज़ा ग़ालिब द्वारा अपना तख़ल्लुस ‘असद‘ रखना भी यही बताता है कि वे भी ऐसा ही चाहते थे। बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने अपना तख़ल्लुस रखा ‘ग़ालिब‘। अरबी में ग़ालिब प्रभु परमेश्वर का ही एक सगुण नाम है। ‘ग़ालिब‘ का अर्थ है ‘प्रभुत्वशाली, सामर्थ्यवान‘।
पवित्र कुरआन में परमेश्वर की सामर्थ्य का परिचय देने के लिए यह शब्द बार-बार प्रयुक्त हुआ है।
ग़ालिब के वालिदैन इस्लामी मान्यताओं पर विश्वास रखने वाले दीनदार मुसलमान थे और ख़ुद उनकी बीवी भी एक निहायत शरीफ़ और दीनदार औरत थीं लेकिन ख़ुद ग़ालिब एक पक्के पियक्कड़ थे। इसके अलावा वे शतरंज, चैपड़ और जुआ भी खेलते थे। मिर्ज़ा जी का एक सितम पेशा डोमनी से इश्क़ भी उनके जीवन की एक ऐसी ही मशहूर घटना है जैसे कि आपके जीवन में दिव्या जी का आना और फिर चला जाना।
मिर्ज़ा ग़ालिब का नज़रिया अपने बारे में
मिर्ज़ा ग़ालिब इस इश्क़ से पहले काम के आदमी हुआ करते थे लेकिन इस कमबख्त इश्क़ ने उन्हें निकम्मा कर दिया था।
‘इश्क़ ने निकम्मा कर दिया ग़ालिब
वर्ना आदमी हम भी थे काम के‘
कहकर उन्होंने ख़ुद बताया है कि इश्क़ ने उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये सभी काम जन्नत में जाने से रूकावट हैं। इस बात को वे जानते थे कि जन्नत में दाख़िल होने के लिए अपने पैदा करने वाले रब का हुक्म मानना और गुनाह से बचना लाज़िमी है, महज़ जन्नत की ख्वाहिश करना या एक मुसलमान के घर पैदा हो जाना या दाढ़ी रखकर कुर्ता-पाजामा और टोपी पहनना या ख़तनाशुदा होना ही काफ़ी नहीं है। उनकी नज़र अपने आमाल पर थी जो कि ख़िलाफ़े इसलाम थे। अपने बुरे आमाल की वजह से वे ख़ुद को कमीना कहते थे।वर्ना आदमी हम भी थे काम के‘
मस्जिद के ज़ेरे साया इक घर बना लिया है
ये बन्दा ए कमीना हमसाया ए ख़ुदा है
ये बन्दा ए कमीना हमसाया ए ख़ुदा है
इसलाम के प्रति ग़ालिब का विश्वास अटल था
इस शेर से यह भी पता चलता है कि उन्हें ख़ुदा के वुजूद पर भी यक़ीन था और उसकी पवित्रता और उसकी महानता का भी। इसीलिए वे हज के लिए काबा जाना तो चाहते थे लेकिन ख़ुदा से अपने आमाल पर शर्मिंदगी का अहसास उनके अंदर बहुत गहरा था। उनके एक शेर से यह देखा जा सकता है।
काबे किस मुंह से जाओगे ‘ग़ालिब‘
शर्म तुमको मगर नहीं आती
इसी तरह उनके बहुत से शेर हैं जिनसे ख़ुदा और इसलाम के प्रति उनके अटल विश्वास को जाना जा सकता है। उन सबके साथ ही ग़ालिब के इस बहुचर्चित शेर को जब रखकर देखा जाता है तभी उनकी हक़ीक़ी मुराद को समझा जा सकता है।शर्म तुमको मगर नहीं आती
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिनदिल के बहलाने को गा़लिब ये ख़याल अच्छा है
एक साहित्यकार का फ़र्ज़ क्या होता है ?
ग़ालिब ने अपने समाज को बर्बादी से निकालने और उसे सही रास्ते पर लाने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि अपने आप को भी वे सही रास्ते पर नहीं ला पाए जबकि वे जानते थे कि सही क्या है ?
न सिर्फ़ यह बल्कि वे एक ऐसा साहित्य छोड़कर गए जो आज भी लोगों को उनके जीवन के असली मक़सद से हटाकर शराब और शबाब की ओर आकर्षित कर रहा है।
आपने लिखा है कि ‘साहित्य की सामाजिक उपादेयता को समझकर ही साहित्योन्मुख हूं। स्मरण रहे साहित्य समाज का दर्पण है और ‘हृदयहीनता की ओर बढ़ रहे कुटुंब का हृदय भी है। धर्म पर आपका अति विश्वास हो सकता है पर मैं ग़ालिब की बात ज़्यादा मुफ़ीद मानता हूं :
‘मुझको मालूम है जन्नत की हक़ीक़त लेकिन
दिल के ख़ुश रखने को ग़ालिब यह ख़याल अच्छा है‘
आपने जो शेर लिखा है, वह दोषपूर्ण है, सही वह है जो मैंने ऊपर लिखा है। इस शेर से आपने भी दूसरों की तरह ग़लत अर्थ ले लिया है। सही भाव वह है जो मैं ऊपर लिख चुका हूं। दिल के ख़ुश रखने को ग़ालिब यह ख़याल अच्छा है‘
यह सही है कि साहित्य समाज का दर्पण है लेकिन इसकी उपादेयता मात्र यही नहीं है। समाज के मार्गदर्शन में साहित्य की एक अहम भूमिका होती है। साहित्य समाज का दर्पण भी होता है और उसे दिशा भी देता है। ऐसा आप भी मानते होंगे।
विचार वस्तु मात्र हैं
साहित्य में विचार होते हैं। विचार भी एक वस्तु है। दूसरी चीज़ों की तरह विचार भी वही सार्थक होता है जो कि उपयोगी हो। कुछ विचार अनुपयोगी भी होते हैं और कुछ विचार घातक होते हैं। अनुपयोगी विचार आदमी की समय और ऊर्जा को नष्ट करते हैं अतः वे भी नुक्सान ही देते हैं। इस तरह उपयोग की दृष्टि से हम विचार को तीन प्रकार में बांट सकते हैं-
1. लाभकारी
2. व्यर्थ
3. घातक
हमारे साहित्य में ये तीनों ही तरह के विचार आपस में मिश्रित हैं और किसी हिंदी साहित्यकार के पास आज तक कोई पैमाना ऐसा न हुआ जिसके ज़रिये यह जानना मुमकिन होता कि कौन सा विचार लाभकारी है और कौन सा घातक ?
साहित्य का प्रभाव समाज पर
कोई भी साहित्य मात्र इस कारण तो लाभकारी नहीं माना जा सकता कि वह साहित्य है, बल्कि साहित्य का आकलन समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव से किया जाता है। लोगों के मन और चरित्र पर वह क्या प्रभाव छोड़ता है ?, उन्हें क्या करने की प्रेरणा देता है ?, उसके प्रभाव में आकर लोग क्या करते हैं ?
इन बातों की बुनियाद पर साहित्य को अच्छा या बुरा कहा जाता है। यदि कोई साहित्य शिल्प की दृष्टि से परफ़ैक्ट है लेकिन उसके प्रभाव में आकर लोग नशे की लत अपना रहे हैं तो उसे अच्छा साहित्य नहीं कहा जा सकता। ग़ालिब के साहित्य पर भी यही बात लागू होती है और आपकी रचनायें मैंने पढ़ी नहीं हैं लेकिन आपकी बात से लगता है कि आप ईश्वर और धर्म को नैतिकता का स्रोत नहीं मानते और न ही इंसान के लिए उनमें विश्वास करना आप इंसान की प्राथमिक आवश्यकता ही मानते हैं।
भूलो मत मूल को
अगर आप अच्छे और बुरे का फ़र्क़ बताने वाले परमेश्वर को ही नज़रअंदाज़ कर देंगे तो फिर आप अपने साहित्य में भी नैतिकता और अच्छाई को क़ायम नहीं रख पाएंगे। ऐसा साहित्य समाज का दर्पण तो अवश्य हो सकता है लेकिन समाज के हितकर हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसे साहित्य का सृजन न केवल आपके जीवन और समय को नष्ट करेगा बल्कि आपके बाद वह हर उस आदमी का समय और चरित्र नष्ट करता रहेगा जो कि उसे पढ़ेगा।
कौन जानता है किसी चीज़ के आख़िरी अंजाम को ?
आप हरगिज़ ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे कि जिसकी अंतिम परिणति आपके लिए और समाज के लिए घातक हो। लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि किस विचार और कर्म की अंतिम परिणति क्या होगी ?
क्योंकि चीज़ें मात्र अपने सामयिक प्रभाव के ऐतबार से ही नहीं देखी जातीं बल्कि वे अपने आख़िरी अंजाम के ऐतबार से भी देखी जाती हैं। कई बार एक बुरा आदमी शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में सारी इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर रख देता है जैसा कि आपके साथ हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आदमी शुरूआती नज़रिये के ऐतबार से किसी को ग़लत समझता है लेकिन बाद में उससे नफ़ा पहुंचता है जैसा कि आपको मुझसे पहुंचा। यह तो समझाने के लिए सामने की मिसाल के तौर पर है वर्ना इससे अच्छी मिसालें मौजूद हैं। यानि कुल मिलाकर इंसान का इल्म इतना कम और कमज़ोर है कि वह नहीं जानता कि जो चीज़ अपने पहले परिचय में भली लग रही है उसका अंजाम क्या होगा ?
हरेक मनभावन चीज़ हितकर नहीं होती
किसी भी चीज़ का मन को भा जाना हरगिज़ यह साबित नहीं करता कि वह लाभकारी भी है और न ही किसी चीज़ से विरक्ति का भाव मन में पाया जाना उसे निरर्थक साबित करने के लिए पर्याप्त है। मन और भावनाएं किसी विचार और वस्तु के नफ़े-नुक्सान को परखने के लिए सिरे से ही कोई कसौटी नहीं हैं, जिन पर कि एक साहित्यकार का सारा दारोमदार होता है।
तब नफ़े-नुक्सान को तय करने का असली पैमाना क्या है ?
जब आप उस पैमाने को दरयाफ़्त कर लेंगे तभी आप लाभकारी साहित्य सृजित करने की क्षमता से लैस हो पाएंगे।
क्या आप बता सकते हैं कि व्यक्ति और समाज के लिए सही-ग़लत और नफ़े-नुक्सान को निर्धारित करने का वास्तिक आधार क्या है ?
और उस तक एक साहित्यकार की हैसियत से आप कैसे पहुंचेगे ?
या आप सिरे से ऐसी कोई कोशिश ही ज़रूरी नहीं समझते ?
संवाद से सत्य की प्राप्ति अभीष्ट है
आप सार्थक साहित्य का सृजन कर सकें इसी कामना से यह संवाद आपके लिए क्रिएट किया गया है।
जो ग़लती ग़ालिब कर चुके हैं उसे दोहराना नहीं है बल्कि उसे सुधारना है। अपने और मानव जाति के बेहतर भविष्य के लिए सही-ग़लत के सही पैमाने का निर्धारण बहुत ज़रूरी है।
पहले भारत में लोग हाथ से या लाठी से नापते थे लेकिन आज नापने का स्टैंडर्ड पैमाना मीटर स्वीकार कर लिया गया है और कोई भी राष्ट्रवादी इस पर आपत्ति नहीं करता कि मीटर तो अंग्रेजों की देन है। जब अंग्रेज़ चले गए तो उनका दिया हुआ मीटर यहां क्या कर रहा है ? ,निकालो उनका मीटर देश से बाहर।
सही-ग़लत का मीटर हमसे लो या फिर हमें दो
अंग्रेज़ों का मीटर, थर्मामीटर और बैरोमीटर ग़र्ज़ यह कि उनके सारे मीटर देशवासी आज भी लिए घूम रहे हैं। जो मीटर उनके पास था वह उन्होंने दे दिया और आपने ले भी लिया लेकिन सही-ग़लत का मीटर उनके भी पास नहीं था और न ही आपके पास है। इसीलिए हिंदू भाई सही-ग़लत तो क्या बताएंगे बल्कि सारे मिलकर भी सही-ग़लत की परिभाषा तक नहीं बता सकते।
ऐसा मैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि एक हक़ीक़त का इज़्हार कर रहा हूं।
जिसे मेरी बात पर ऐतराज़ हो वह मेरे सवाल का सवाल का जवाब देकर दिखाए।
अगर अंग्रेजों के भौतिक मीटर आप ले सकते हैं तो फिर मुसलमानों आप सही-ग़लत नापने का मीटर क्यों नहीं ले सकते ?
अगर आपके पास पहले से ही मौजूद है तो फिर उसे सामने लाईये और हमें भी दीजिए।
आपका मीटर अच्छा हुआ तो हम भी उससे काम लेंगे।
‘वसुधैव कुटुंबकम्‘ : परिवार एक है तो उसका मीटर भी एक हो
अब सारी दुनिया में चीज़ों को नापने और जांचने के मीटर एक हो चुके हैं और विचार भी वस्तु होते हैं लिहाज़ा विचारों को नापने और जांचने के लिए भी कम से कम एक मीटर तो होना ही चाहिए और अगर समाज में बहुत से मीटर प्रचलित हों तो उनमें से जो बेहतर हो उसे सारे विश्व समाज के लिए स्टैंडर्ड मान लिया जाना चाहिए।
भौतिक क्षेत्र में ऐसा हो चुका है। अब सूक्ष्म भाव जगत में भी इस प्रयोग को आज़माने का वक्त आ चुका है। मेरा मिशन यही है। मानव जाति का एकत्व ही मेरा लक्ष्य है। कोई भी बंटवारा मुझे हरगिज़ मंज़ूर नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए।
नोट - भाई अमरेंद्र से इस संवाद की पूरी पृष्ठभूमि जानने के लिए देखें उनकी टिप्पणी डा. दिव्या जी के संबंध में।

.png) Hire Us
Hire Us